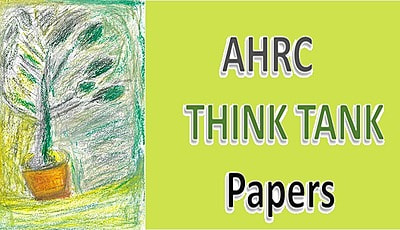INDIA:नर्मदा जल सत्याग्रह – केवल जमीन का नहीं न्याय का आग्रह
 गोघल गाँव और खरदना गाँव में 200 लोग 17 दिनों तक नर्मदा नदी में ठुड्डी तक भरे पानी में खड़े रहे। वे कोई विश्व रिकार्ड नहीं बनाना चाहते थे। उन्हे अखबार में भी अपना चित्र नहीं छपवाना था। उन्हे विकास के नाम पर जल समाधि दी जा रही थी, जिसके विरोध में उन्होने जल सत्याग्रह शुरू किया। वे कह रहे थे यदि देश के विकास के लिए बांध बना है तो उनके जीवन के अधिकार को क्यों ख़त्म किया जा रहा है? वे संसाधनों पर अधिकार चाहते थे क्यूंकि जमीन, पानी और प्राकृतिक संसाधन की उनके जीवन के अधिकार का आधार हैं। मध्यप्रदेश में दो बडे बाँध – इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बाँध है। इन बांधों से बिजली बनती है और कुछ सिंचाई भी होती है। इन बांधों के दायरे के बाहर की दुनिया को इन बांधों से बिजली मिलती है और उनके घर इससे रोशन होते हैं। रेलगाड़ियाँ भी चलती है। ये बिजली सबसे ज्यादा रोशन करती है नए भारत के शहरों को, उन उद्योगों को, जो रोज़गार खाते हैं, माल्स और हवाई अड्डों को। खरगोन, खंडवा, हरदा, देवास ये वे जिले हैं जहाँ लगभग 2 लाख परिवारों को उनकी जड़ों से उखाड़ा गया यानी सरकार ने उनकी दुनिया का अधिग्रहण कर लिया है। यह एक अध्यादेश होता है जो बात तो करता है जमीन के एक टुकडे की परन्तु सच में वह एक ऐसा दस्तावेज होता है जो लोगों को बताता है कि देश और समाज (शहर और एक ख़ास वर्ग) की विलासिता के लिए तुम्हे बलिदान देना होगा। स्वतंत्रता के बाद से लगतार देश में लोगों को विस्थापित किया जाता रहा है; विस्थापन के शिकार आदिवासी, दलित और भूमिहीन सबसे ज्यादा रहे, क्यूंकि सम्पत्तिवान लोगों की संख्या हमेशा से कम रही और सरकार ने उन्हे उनके प्रभावों के चलते उन्हे हमेशा कुछ हद तक सुविधाएं दीं। इन बांधों या किसी और भी परियोजना में जिन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा उनकी जिन्दगी प्राकृतिक संसाधनों जैसे – जमीन, पानी, जंगल और पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर रही है। वे मुद्रा यानी नकद यानी कागज़ की सम्पदा में रमते ही नहीं हैं। ऐसे में उन्हे उनकी जमीनों के बदले मुआवजे के तौर पर नकद राशि देने की व्यवस्था बनायी गयी। यह सरकार के हिसाब से सबसे सस्ता, आसान और सहज विकल्प था; परन्तु लोगों के लिए बहुत कठिन और जीवन ख़त्म कर देने वाला विकल्प; एक उदाहरण देखिये। 1980 के दशक में जब रानी अवंती बाई परियोजना यानी बरगी बाँध बना, तब लोगों को 800 से 1500 रूपए प्रति एकड़ के मान से मुआवजा दिया गया। जैसे ही आस-पास के लोगों को पता चला तो सभी यह मानने लगे अब तो विस्थापित जमीन खरीदेंगे, ये उनकी मजबूरी है। और दो तीन दिनों के भीतर वहां जमीन के दाम बढे। एक हज़ार रूपए एकड़ की जमीन कुछ दिनों में 3500 रूपए की कीमत तक पंहुच गयी। लोगों को जो नकद राशि मिली थी उसके कोई मायने ही नहीं रह गए। सरदार सरोवर में मिले नकद मुआवजे से जमीन खरीदने के लिए जो व्यवस्था बनाई गयी उसमे पटवारी से लेकर राजस्व अधिकारी, वकीलों और भू-अर्जन अधिकारी के गिरोह को सक्रीय कर दिया। जिन्होने मिलकर आदिवासियों और विस्थापितों के चील-कौयों की तरह नोचा। सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला गया और मध्यप्रदेश सरकार कहती रही हमारे पास परियोजना प्रभावितों को देने के लिए जमीन नहीं है; पर डुबोने के लिए जमीन थी। जमीन तो थी और है भी। यदि सरकार की मंशा होती तो परियोजना प्रभावितों का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह का सम्मान होता। उन्हे सामान्य इंसान से थोडा तो ज्यादा माना ही जाता। उन्हे अपने ही देश में गैर-कानूनी अप्रवासी और अतिक्रमणकारी और अधूरे नागरिक का दर्ज़ा नहीं दिया जाता। जो अपनी पूरी सम्पदा देश के विकास के लिए दे रहा है, क्या उसके लिए बेदखली की प्रक्रिया चलाना कोई न्यायोचित कृत्य है। क्या है इनकी अपेक्षाएं – भूमिहीनों के लिए एक निर्धारित सम्मानजनक नकद राशि और जमीन के बदले जमीन; बस यही न। जमीन आज भारत के भीतर पनप रहे नए उपनिवेशों के लिए ताकतवर होने का नया हथियार है। देश 8000 लोग भारत के सकल घरेलु उत्पाद के 70 फ़ीसदी हिस्से पर कब्ज़ा रखते हैं। इस कब्ज़े में सबसे बड़ा हिस्सा जमीनों, पहाड़ों और नदियों पर कब्जे का है। इनकी सत्ता की ताकत इतनी ज्यादा है कि चुनी हुई सरकार भी इनकी अनुमति के बिना कोई नीति नहीं बना सकती है। पूँजी की यही व्यवस्था तय करती है प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों का या कहें कि समुदाय का कोई हक़ नहीं होगा। खनिज संसाधनों के दोहन, जिसमे हमने देखा कि उडीसा, झारखंड, छतीसगढ़ में २४ लाख हेक्टेयर जमीन पर 20 कंपनियों ने नज़र डाली। उस पर उन्हे कब्ज़ा चाहिए था तो सरकार ने 6 लाख आदिवासियों को जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया। उन्हे आतंकित किया गया, गोलियां चली, बलात्कार किये गए, यानी हर वह काम किया गया जिससे लोगों में सत्ता और पूँजी का आतंक बैठाया जा सके और वह संसाधनों की लूट की नीतियों का विरोध करने का विचार भी न कर सकें। मध्यप्रदेश का सिंगरौली जिला देश की उर्जा राजधानी बना और साथ ही देश का सबसे प्रदूषित शहर भी, पर 2011 की जनगणना के मुताबिक़ इसी जिले के 90 प्रतिशत लोग मिट्टी के तेल यानी केरोसीन के अपने घरों को रोशन करते हैं। जिस इलाके से विकास की धारा बहाई जाती है वह इलाका आम लोगों के नज़रिए से मौत के भय और सत्ता के प्रति अविश्वास के क्यों भर जाता है?
गोघल गाँव और खरदना गाँव में 200 लोग 17 दिनों तक नर्मदा नदी में ठुड्डी तक भरे पानी में खड़े रहे। वे कोई विश्व रिकार्ड नहीं बनाना चाहते थे। उन्हे अखबार में भी अपना चित्र नहीं छपवाना था। उन्हे विकास के नाम पर जल समाधि दी जा रही थी, जिसके विरोध में उन्होने जल सत्याग्रह शुरू किया। वे कह रहे थे यदि देश के विकास के लिए बांध बना है तो उनके जीवन के अधिकार को क्यों ख़त्म किया जा रहा है? वे संसाधनों पर अधिकार चाहते थे क्यूंकि जमीन, पानी और प्राकृतिक संसाधन की उनके जीवन के अधिकार का आधार हैं। मध्यप्रदेश में दो बडे बाँध – इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बाँध है। इन बांधों से बिजली बनती है और कुछ सिंचाई भी होती है। इन बांधों के दायरे के बाहर की दुनिया को इन बांधों से बिजली मिलती है और उनके घर इससे रोशन होते हैं। रेलगाड़ियाँ भी चलती है। ये बिजली सबसे ज्यादा रोशन करती है नए भारत के शहरों को, उन उद्योगों को, जो रोज़गार खाते हैं, माल्स और हवाई अड्डों को। खरगोन, खंडवा, हरदा, देवास ये वे जिले हैं जहाँ लगभग 2 लाख परिवारों को उनकी जड़ों से उखाड़ा गया यानी सरकार ने उनकी दुनिया का अधिग्रहण कर लिया है। यह एक अध्यादेश होता है जो बात तो करता है जमीन के एक टुकडे की परन्तु सच में वह एक ऐसा दस्तावेज होता है जो लोगों को बताता है कि देश और समाज (शहर और एक ख़ास वर्ग) की विलासिता के लिए तुम्हे बलिदान देना होगा। स्वतंत्रता के बाद से लगतार देश में लोगों को विस्थापित किया जाता रहा है; विस्थापन के शिकार आदिवासी, दलित और भूमिहीन सबसे ज्यादा रहे, क्यूंकि सम्पत्तिवान लोगों की संख्या हमेशा से कम रही और सरकार ने उन्हे उनके प्रभावों के चलते उन्हे हमेशा कुछ हद तक सुविधाएं दीं। इन बांधों या किसी और भी परियोजना में जिन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा उनकी जिन्दगी प्राकृतिक संसाधनों जैसे – जमीन, पानी, जंगल और पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर रही है। वे मुद्रा यानी नकद यानी कागज़ की सम्पदा में रमते ही नहीं हैं। ऐसे में उन्हे उनकी जमीनों के बदले मुआवजे के तौर पर नकद राशि देने की व्यवस्था बनायी गयी। यह सरकार के हिसाब से सबसे सस्ता, आसान और सहज विकल्प था; परन्तु लोगों के लिए बहुत कठिन और जीवन ख़त्म कर देने वाला विकल्प; एक उदाहरण देखिये। 1980 के दशक में जब रानी अवंती बाई परियोजना यानी बरगी बाँध बना, तब लोगों को 800 से 1500 रूपए प्रति एकड़ के मान से मुआवजा दिया गया। जैसे ही आस-पास के लोगों को पता चला तो सभी यह मानने लगे अब तो विस्थापित जमीन खरीदेंगे, ये उनकी मजबूरी है। और दो तीन दिनों के भीतर वहां जमीन के दाम बढे। एक हज़ार रूपए एकड़ की जमीन कुछ दिनों में 3500 रूपए की कीमत तक पंहुच गयी। लोगों को जो नकद राशि मिली थी उसके कोई मायने ही नहीं रह गए। सरदार सरोवर में मिले नकद मुआवजे से जमीन खरीदने के लिए जो व्यवस्था बनाई गयी उसमे पटवारी से लेकर राजस्व अधिकारी, वकीलों और भू-अर्जन अधिकारी के गिरोह को सक्रीय कर दिया। जिन्होने मिलकर आदिवासियों और विस्थापितों के चील-कौयों की तरह नोचा। सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला गया और मध्यप्रदेश सरकार कहती रही हमारे पास परियोजना प्रभावितों को देने के लिए जमीन नहीं है; पर डुबोने के लिए जमीन थी। जमीन तो थी और है भी। यदि सरकार की मंशा होती तो परियोजना प्रभावितों का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह का सम्मान होता। उन्हे सामान्य इंसान से थोडा तो ज्यादा माना ही जाता। उन्हे अपने ही देश में गैर-कानूनी अप्रवासी और अतिक्रमणकारी और अधूरे नागरिक का दर्ज़ा नहीं दिया जाता। जो अपनी पूरी सम्पदा देश के विकास के लिए दे रहा है, क्या उसके लिए बेदखली की प्रक्रिया चलाना कोई न्यायोचित कृत्य है। क्या है इनकी अपेक्षाएं – भूमिहीनों के लिए एक निर्धारित सम्मानजनक नकद राशि और जमीन के बदले जमीन; बस यही न। जमीन आज भारत के भीतर पनप रहे नए उपनिवेशों के लिए ताकतवर होने का नया हथियार है। देश 8000 लोग भारत के सकल घरेलु उत्पाद के 70 फ़ीसदी हिस्से पर कब्ज़ा रखते हैं। इस कब्ज़े में सबसे बड़ा हिस्सा जमीनों, पहाड़ों और नदियों पर कब्जे का है। इनकी सत्ता की ताकत इतनी ज्यादा है कि चुनी हुई सरकार भी इनकी अनुमति के बिना कोई नीति नहीं बना सकती है। पूँजी की यही व्यवस्था तय करती है प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों का या कहें कि समुदाय का कोई हक़ नहीं होगा। खनिज संसाधनों के दोहन, जिसमे हमने देखा कि उडीसा, झारखंड, छतीसगढ़ में २४ लाख हेक्टेयर जमीन पर 20 कंपनियों ने नज़र डाली। उस पर उन्हे कब्ज़ा चाहिए था तो सरकार ने 6 लाख आदिवासियों को जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया। उन्हे आतंकित किया गया, गोलियां चली, बलात्कार किये गए, यानी हर वह काम किया गया जिससे लोगों में सत्ता और पूँजी का आतंक बैठाया जा सके और वह संसाधनों की लूट की नीतियों का विरोध करने का विचार भी न कर सकें। मध्यप्रदेश का सिंगरौली जिला देश की उर्जा राजधानी बना और साथ ही देश का सबसे प्रदूषित शहर भी, पर 2011 की जनगणना के मुताबिक़ इसी जिले के 90 प्रतिशत लोग मिट्टी के तेल यानी केरोसीन के अपने घरों को रोशन करते हैं। जिस इलाके से विकास की धारा बहाई जाती है वह इलाका आम लोगों के नज़रिए से मौत के भय और सत्ता के प्रति अविश्वास के क्यों भर जाता है?
 सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना से ही अधोसंरचनात्मक विकास की नीतियां बनाना शुरू की। 1951 में बनी पहली पंचवर्षीय योजना से ही यह तय हो गया कि देश के गाँवों और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण से ही हमारे विकास का ढांचा खडे होने वाला है। यह तय था कि इसके लिए लोगों का विस्थापन होगा। विस्थापन हुआ भी। भाखड़ा नंगल और हीराकुंड बांधों से बड़ी परियोजनाओं की पक्रिया शुरू हुई; पर एक भी दस्तावेज में यह उल्लेख नहीं किया गया कि जिनका विस्थापन होगा, उनका पुनर्वास भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। पंडित नेहरु ने इन्हे आधुनिक विकास का मंदिर कहा उन्होने यह कभी नहीं कहा कि विस्थापितों को हमें पूजना और सम्मानित करना होगा; पर सच यह था कि इन मंदिरों के निर्माण की नीव डालने के लिए समाज और प्रकृति की जड़ें खोद डाली गयीं। नींव में पत्थर नहीं डले, आदिवासियों और ग्रामीणों के शरीर की हड्डियाँ डाली गयी, और उनके विश्वास को बारीक करके जमीन में दबाया गया। इस देश में 5177 बड़ी विकास परियोजनाएं चल रही हैं; परन्तु कभी भी यह जानकारी संकलित नहीं की गयी कि कहाँ, कौन विस्थापित हो रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं, विस्थापन के बाद उनकी जिन्दगी का क्या हुआ? लोग जिंदा भी हैं या नहीं!
सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना से ही अधोसंरचनात्मक विकास की नीतियां बनाना शुरू की। 1951 में बनी पहली पंचवर्षीय योजना से ही यह तय हो गया कि देश के गाँवों और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण से ही हमारे विकास का ढांचा खडे होने वाला है। यह तय था कि इसके लिए लोगों का विस्थापन होगा। विस्थापन हुआ भी। भाखड़ा नंगल और हीराकुंड बांधों से बड़ी परियोजनाओं की पक्रिया शुरू हुई; पर एक भी दस्तावेज में यह उल्लेख नहीं किया गया कि जिनका विस्थापन होगा, उनका पुनर्वास भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। पंडित नेहरु ने इन्हे आधुनिक विकास का मंदिर कहा उन्होने यह कभी नहीं कहा कि विस्थापितों को हमें पूजना और सम्मानित करना होगा; पर सच यह था कि इन मंदिरों के निर्माण की नीव डालने के लिए समाज और प्रकृति की जड़ें खोद डाली गयीं। नींव में पत्थर नहीं डले, आदिवासियों और ग्रामीणों के शरीर की हड्डियाँ डाली गयी, और उनके विश्वास को बारीक करके जमीन में दबाया गया। इस देश में 5177 बड़ी विकास परियोजनाएं चल रही हैं; परन्तु कभी भी यह जानकारी संकलित नहीं की गयी कि कहाँ, कौन विस्थापित हो रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं, विस्थापन के बाद उनकी जिन्दगी का क्या हुआ? लोग जिंदा भी हैं या नहीं!
यानी बात यह कि आज तक भारत में यह कोई समग्र आंकड़ा ही नहीं है कि किस परियोजना में कितने लोगों का विस्थापन हुआ और आज वे किस हाल में हैं; इसका मतलब है कि सरकार ने हमेशा यह चाहा है कि ये तो मर ही जाएँ तो अच्छा है; हम इनके लिए हैं ही नहीं; यही कारण है कि जल सत्याग्रह के 13 दिनों तक सरकार लोगों पास नहीं गयी। फिर बात शुरू हुई और बड़ी ही कुटिलता के साथ उन्होने ओंकारेश्वर यानी एक बाँध के तहत जमीन देने की बात मान ली, पर दूसरे बाँध यानी इंदिरा सागर की बात को फिर से नकार दिया।
प्रतिबद्धताएं बहुत स्पष्ट हैं; बाँध और विकास परियोजनाओं की बेदी पर बलि चढ़ाये जाने वाले लोगों, जिनमे 65 प्रतिशत आदिवासी और दलित हैं; के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। वर्ष 2007 से 2012 के बीच निवेश के नाम पर साढ़े चार लाख हेक्टेयर जमीन की व्यवस्था कर दी चुकी है। एक आवेदन पर हज़ारों एकड़ जमीन उद्योगों और जमीन के कारोबारियों को देने के व्यवस्था बना दी गयी। 8 सितम्बर 2012 को, जब लोग अपने लिए जमीन की मांग कर रहे थे थी उसी दिन भोपाल में कलेक्टर्स-कमिश्नर्स की कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने अफसरों को निर्देश दिया है कि 15 सितम्बर 2012 तक 26000 हेक्टेयर जमीन 26 जिलों में निकालें और उद्योगों विभाग को हस्तांतरित कर दें ताकि कंपनियों को जमीन दी जा सके। एक भी उदहारण सरकार का वंचितों और गरीबों के पक्ष में बता दें जब सरकार ने कहा हो कि इस तारीख तक वन अधिकार क़ानून के तहत वनों पर हक़ दे दें, राशन कार्ड इस तारीख तक बना दें, या दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दें; नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ; जहाँ लूट है, वहां सरकार भी समयबद्ध और प्रतिबद्ध हो जाती है;
जिन परियोजनाओं की बात आज हो रही है उन परियोजनाओं में भी यह आज तक तय नहीं हो पाया कि कितने गाँव और कितने जंगल और कितने लोग डूबेंगे; ऐसे में किस सरकार की बात कर रहे हैं हम? यह सरकार एक मृगतृष्णा है; जो नज़र आता है वह होता ही नहीं है; लोकतंत्र में विकास का मतलब यह नहीं कि 80 प्रतिशत को बिजली देने के लिए आपको बाकी के 20 प्रतिशत की हत्या कर देने का अधिकार है; यदि उन 20 फीसदी का सही पुनर्वास नहीं होगा तो किसी को भी सुकून से उस बिजली से वातानुकूलित यन्त्र चलाने का नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए; एक भी परियोजना ऐसी नहीं है जिसके बारे में तथाकथित विशेषज्ञ सही आंकलन करके बता पाए हों कि इसके चलते जैव विविधता और पारिस्थितिकीय व्यवस्था का कितना नुकसान होगा। जब समुदाय ने यह बताने की कोशिश की तो उसे विकास विरोधी और राष्ट्रद्रोह के मुकदमों में फंसाया गया। और फिर राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंत्री ने सन्देश दिया कि ये मुट्ठीभर जल सत्याग्रही हमें कमज़ोर न समझे। हमें सरकार चलाना आता है और हम दबेंगे नहीं। हम अपना काम करेंगे। और ठीक 20 घंटे के बाद पुलिस बल ने ताकत का प्रयोग करने सत्य के आग्रह को ठुकरा दिया।
लोग गोघलगाँव और खरदना में 15 से 17 दिन पानी में इसलिए खड़े रहे ताकि उनकी बात सुनी जाए। जो इंसानी तरीकों से तो व्यवस्था सुन ही नहीं रही थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और पुनर्वास की नीति है कि जब तक पुनर्वास पूरा नहीं होगा तब तक बांधों में जलभराव के स्तर को इंदिरा सागर में 260 मीटर और ओंकारेश्वर में 189 मीटर तक रखा जाएगा परन्तु इन बांधों में दो मीटर से ज्यादा जलभराव का स्तर बढ़ा दिया गया, जिनसे 100 ऐसे गांव प्रभावित हुए जिनका सर्वे तक नहीं हुआ था। खेत, जंगल और घर डूब में आये। यह सरकार और योजनाकारों की रणनीति होती है। पुनर्वास की प्रक्रिया को वे विलम्ब करते जाते हैं और दूसरी तरफ जल स्तर बढाते जाते हैं ताकी जमीनें डूबती जाएँ। जब घर और जमीन ही डूब जाते हैं तो फिर सर्वे नहीं हो पाता है। तब जमीनी स्तर पर भूअर्जन अधिकार, पटवारी, पंजीयक और स्थानीय प्रशासन का गठजोड़ ग्रामीणों की जिन्दगी में से संभावनाओं की आख़िरी बूँद तक निचोड़ लेता है। जिनका सब कुछ डूब रहा होता है वे कर्जे लेकर इन अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। औरतें अपने घर के बर्तन और गहने बेंचने को मजबूर हुई। सिर्फ इस उम्मीद पर कि यदि जमीन मिल गयी तो जिन्दगी चल जायेगी। सरदार सरोवर परियोजना में नकद मुआवजे और जमीन की खरीदी में अब तक 600 करोड़ रूपए का घोटाला और भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। ऐसे में हमें न्याय की परिभाषा और भारत की राजनीतिक व्यवस्था के चरित्र पर सवाल उठाने ही होंगे। जब विकास की रूप रेखा बनायी जाती है, तब क्या न्याय उसका मूल सूचक और अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए? बिना न्याय क्या कोई भी विकास संभव है? इंदिरा सागर और ओम्कारेश्वर बाँध परियोजनाएं तो यह बताती हैं कि जितना ज्यादा अन्याय होगा, विकास का चेहरा उतना ज्यादा उजला माना जाएगा। न्याय का मतलब केवल लोगों को जमीन मिलना नहीं है। न्याय का मतलब है समाज का राज्य की व्यवस्था में विश्वास होना कि वह यानी राज्य उसे बलि नहीं चढ़ाएगा। उसके दुखों को समझेगा और उसे मारने के लिए रणनीतिगत अनुष्ठान नहीं करेगा। न्याय का मतलब जिम्मेदारी के साथ पारिस्थितिकीय तंत्र का व्यवस्थापन करना, न्याय का मतलब है केवल इंसानी जरूरतों की पूर्ति के लिए काम न करना; बल्कि यह भी सुनिश्चित करना कि प्रकृति का संतुलन बना रहे। यदि कोई विकास एक सुखी जीवन और समानता के वातावरण को महत्व न दे, तो मान कर चलिए कि वह इमारत बेहद कमज़ोर नींव पर खड़ी है।
उत्तरपूर्व के राज्यों में 100 बाँध बन रहे हैं, उत्तराखंड में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को बांधों से बाँध दिया गया है। अब वह एक ठंडा इलाका नहीं रह गया है। वहां पहाड़ों पर आग जल रही है और पहाड़ तप रहे हैं। मध्यप्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड इलाकों में 15 सालों से बार-बार सूखा पड़ रहा है, वहां विकास के लिए बनी नीति में थर्मल उर्जा के 30 सयंत्र लगाए जा रहे हैं, कोड़ा कुलम में हज़ारों लोग कह रहे हैं परमाणु संयंत्र मानव सभ्यता को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए परमाणु संयंत्र मत लगाओ; जो भी यह कह रहा है कि बिजली पैदा करने के लिए हम दुनिया में स्थायी अँधेरा लाने की और बढ़ रहे हैं इसे रोका जाए; उसे सरकार और पूँजी के समर्थक राष्ट्रद्रोही करार दे रहे हैं। ऊर्जा के नाम पर जिस तरह का पागलपन दर्शाया जा रहा है वह विकास की सोच में आ चुकी विकृति को दर्शाता है। किसके लिये इस बिजली का उत्पादन होगा? देश में 60 प्रतिशत बिजली ६०० उद्योगों, माल और एअरपोर्ट द्वारा उपयोग की जाती है पर इसके लिये पिछले 50 वर्षों में 6 करोड लोगों को विस्थापित किया जा चुका है और उनकी जमीन और जंगल डुबोए जा चुके हैं। उनसे अपेक्षा है कि वे सब कुछ डूब जाने के बाद भी चुप रहें। जब नर्मदा घाटी में लोग, जिनका सब कुछ उजड़ा है, जमीन मांगते हैं तो मुख्यमंत्री, केबिनेट मंत्री से लेकर नौकरशाही और उसी पक्ष के पत्रकार बुद्धिजीवी यह कहने लगते हैं कि ये लोग विकास विरोधी हैं और उनकी मांगे जायज़ नहीं हैं। सच तो यही है कि हमारी पक्षधरता क्या है; हम किसके पक्ष में हैं; आखिर जायज़ और नाजायज़ का निर्धारण कौन करेगा? जब पानी में बैठ- बैठे उनकी चमड़ी और अंग गलने लगे तो मानवीयता और नैतिकता का सवाल उठाया जाने लगा। कहा गया कि सरकार पर दबाव बनाने का यह तरीका आपराधिक है। एक पत्रकार ने लिखा जब हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया है तो विरोध के नाम पर लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाना गलत है। ये गंभीर अपराध है। सरकार ने हरदा में जो कदम उठाया (700 पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के जबरदस्ती पानी से निकल दिया और वहां धारा 144 लगा दी ताकि लोग इकठ्ठा न हो सकें) वही कदम उसे खंडवा में भी उठाना था। असहमति और बहस के हर नजरिए के लिए भरपूर गुंजाईश है। बहस होती रहना चाहिए। विरोध होते रहना चाहिए लेकिन आत्म उत्पीड़न का ये तरीका गलत है इसे जब जब दुहराया जाए सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। यहाँ सवाल यह उठता है कि जब लोगों ने इस तरह प्रदर्शन का निर्णय लिया होगा तब उनकी मनः स्थिति क्या रहो होगी, क्या यह हम कल्पना कर सकते हैं? शायद कुछ लोगों के लिए अब हर लड़ाई आखिरी लड़ाई बन गयी है, नहीं तो कौन आत्महत्या करना चाहेगा; सब कुछ खो जाता है तब लोग फिर से बनाने की चाहत रखते हैं; पर जब यह लगने लगे कि उन्हे फिर से जिन्दगी खड़ी नहीं करने दी जायेगी; तब विचार यही होता है कि अब बस आखिरी लड़ाई है। इस पूरी लड़ाई में शहर का समाज परियोजना प्रभावितों को अपना दुश्मन मानता है। वह उन परिवारों की पीड़ा को महसूस करने को तैयार ही नहीं है। जब विस्थापितों की बात उनकी गाँव में नहीं सुनी जाती है तभी वे जिला मुख्यालय आते हैं और शायद आखिर में राजधानी में। और जब ये आते हैं तो बजाये इनके साथ खडे होने के, इनके गरियाया जाता है; क्यूंकि शहर के सड़क कुछ घंटों के लिए रुक सी जाती है। हम लोग शापिंग के लिए नहीं जा पाते हैं। वे भूल जाते हैं कि लकड़ी की आग की तरह ही अन्याय की आग भी एक स्तर से बाद यह भेद नहीं करती है कि उसे किसी को जलना है और किसी को नहीं। वह सबको जलाती है। गाँव की यह आग शहर तक भी पंहुचेगी एक दिन। हम उस स्थिति को क्या कहेंगे जब राज्य के कुछ हिस्से समाज को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे और समाज का हक़ उसे अपना विरोध लगने लगे। नर्मदा के मामले में पूरा राज्य (यानी स्टेट) तो लोगों के खिलाफ नहीं हुआ पर राज्य के कुछ हिस्से; मंत्री, जनप्रतिनिधि और अफसरान जरूर लोगों के हकों को राज्य के अहम् का विषय बनाते नज़र आये। जब भी राज्य की नीति पर सवाल उठते हैं; तब यह होना स्वाभाविक है कि जिनके हित प्रभावित होंगे वे सत्याग्रह को भी टकराव और अहम् का विषय बनायेंगे ही। ऐसे में सहूलियत में जीने वाला व्यापक समाज का एक हिस्सा सत्याग्रह और सत्याग्रहियों के खिलाफ होते जाता है।
एक वक्त आता है जब अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई लोगों की जिन्दगी की आखिरी लड़ाई बन जाती है। शायद कुछ लोगों के लिए अब हर लड़ाई आखिरी लड़ाई बन गयी है, नहीं तो कौन आत्महत्या करना चाहेगा; सब कुछ खो जाता है तब लोग बनाने की चाहत रखते हैं; पर जब यह लगने लगे कि उन्हे फिर से जिन्दगी खड़ी नहीं करने दी जायेगी; तब विचार यही होता है कि अब बस आखिरी लड़ाई है; भूखे और उजडे हुए लोगों को संविधान की किताब मत दिखाईएगा; ये किताब उन मंत्रियों और मुख्यमंत्री को दिखाइए जो इसके पन्नों को बार बार फाडते हैं।
उपनिवेशवादी व्यवस्था, यानी जब हम पर कोई बाहर की ताकत शासन करती है, तब सरकार कहती है कि हम व्यापक हितों और व्यवस्थापन के लिए नीतियां बनाते हैं। हमारी सरकार भी आज यही कहती है हम छोटे समूह या कुछ लोगों के हितों को पूरा करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमें तो व्यापक हित और राज्य के विकास को महत्व देना है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या किसी विकास से यदि किसी भी समूह, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, का अहित होता हो या उसका जीवन असहज और सुरक्षित होता ही, तो क्या वह विकास व्यापक समाज का हित कर पायेगा? यदि बीज जहरीला या कमज़ोर होगा तो वृक्ष मीठे और जनहित के फल कैसे पैदा कर सकता है! इसका मतलब यह भी है कि हम विकास के नाम पर आज भी उपनिवेशवादी मानसिकता को शासन व्यवस्था के केंद्र में रखे हुए हैं।
About the Author: Mr. Sachin Kumar Jain is a development journalist, researcher associated with the Right to Food Campaign in India and works with Vikas Samvad, AHRC’s partner organisation in Bophal, Madhya Pradesh. The author could be contacted at sachin.vikassamvad@gmail.com Telephone: 00 91 9977704847