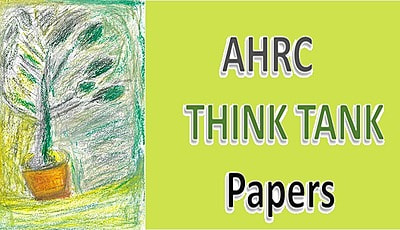INDIA: बदलाव से पहले सही आंकड़े तो सामने लाईये
हमें अपनी नयी सरकार से सामान्य ज्ञान का एक सवाल पूछना चहिये कि यदि हमारे यहाँ नीतियां किस आधार पर बनती हैं, जबकि कई मूल विषयों पर भारत में आंकडें और जानकारियां एकत्र करने में परहेज किया जाता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र से लेकर आर्थिक सूचकांकों, कुपोषण और विस्थापन तक ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, जहाँ आंकड़ों और ताज़ा जानकारियों के प्रबंधन की कोई व्यवस्था ही नहीं है. इसका मतलब यह कि हम सरकार की किसी भी पहल और उसके परिणामों को विश्वसनीय नहीं मान सकते है. जो भी हुआ या हो रहा है, वह सच नहीं है, क्योंकि उसे सही आंकड़ों के अभाव में जांचना संभव ही नहीं है.
भारत में लोग वास्तव में कितना कमाते हैं उसकी जानकारी ही इकठ्ठा नहीं होती है. और बात की जाती है उनकी कमाई बढाने की. हमारे यहाँ जो भी जानकारियां है वह व्यय पर आधारित है. एन एस एस ओ भी प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग, व्यय की ही जानकारी इकठ्ठा करता है.
हमारा वित्त मंत्रालय हर साल आर्थिक वृद्धि के सूचक के रूप में बताता है कि देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ गयी है, परन्तु वह लोगों की आर्थिक परिस्थितियों एक सही आंकलन नहीं होता है, क्योंकि वह आय का औसत आंकलन होता है. एक व्यक्ति की वास्तविक वार्षिक आय 100 करोड़ रूपए, दूसरे व्यक्ति की आय 5 करोड़ रूपए, तीसरे व्यक्ति की आय 50 लाख रूपए, चौथे व्यक्ति की आय 5 लाख रूपए, पांचवे व्यक्ति की आय 1 लाख रूपए, छठवें व्यक्ति की आय 24 हज़ार रूपए, सातवें व्यक्ति की आय 20 हज़ार रूपए और आठवें, नवमें, दसवें व्यक्ति की आय 12 हज़ार रूपए है. इस मान से हमारी औसत आय हो गयी १०.५५६८ करोड़ रूपए. अब सवाल यह है कि इस आंकलन में आखिरी के 5 व्यक्तियों की वास्तविक स्थिति झलकती है या नहीं? यहाँ तक कि भारत में गरीबी का आंकलन भी व्यक्ति की आय के मानक (कि एक व्यक्ति की कम से कम कितनी आय होनी चाहिए) के आधार पर नहीं होता है. यह आंकलन केवल व्यय के आधार पर होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति 22 रूपए से कम गाँव में या 28 रूपए से काम शहर में काम खर्च कर रहा है, तो उसे गरीब मान लिया जाएगा.
अब जरा इस बात पर विचार कीजिये. भारत में भुखमरी और कुपोषण एक बड़ा राजनीतिक, सामाजिक और अकादमिक सवाल बना हुआ है, लेकिन आज यानी 2014 में भी जब हम इन विषयों पर बहस करते हैं या कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम बनाने की पहल करते हैं, तब हमें वर्ष 2005-06 में सम्पादित हुए राष्ट्रीय परिवार स्वस्थ्य सर्वेक्षण का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि पिछले 8 सालों में हमारी सरकार ने कुपोषण और स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों की पड़ताल के लिए कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किये ही नहीं. ऐसे में यही अहसास होता है कि वास्तव में सरकारें भुखमरी, कुपोषण और गरीबी के सन्दर्भ में साक्ष्य आधारित पहल करने के बजाये सतही और गैर-जवाबदेय पहल करते रहना चाहती हैं.
इसके साथ ही दूसरा मसला आंकड़ों और जानकारियों की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है. मध्यप्रदेश की शिशु मृत्यु दर 56 है, यानी जब एक हज़ार जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, तब एक वर्ष से काम उम्र के 56 बच्चों के मध्यप्रदेश में मृत्यु हो जाती है, वास्तव में यह एक आंकलन होता है, जिसकी वास्तविक वास्तविक आंकड़ों के साथ पड़ताल की जाना चाहिए. जब एक हज़ार जीवित जन्म पर 56 बच्चों की मृत्यु होती है, तो 15 लाख जीवित जन्म पर 84000 बच्चों की मृत्यु हो रही है. इस आंकलन के ठीक उलट मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2013-14 के लिए जो आंकड़े दर्ज किये, उनके आधार पर राज्य में लगभग 7800 शिशु मृत्यु हुई. इस हिसाब से तो मध्यप्रदेश की शिशु मृत्यु दर लगभग 5 होना चहिये, जो की दुनिया के सबसे विकसित देशों की दर है. विडम्बना यह है कि हमारे यहाँ हर महीने जिला स्तर पर, हर तीन महीने में राज्य स्तर पर और सालाना मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षाएं होती हैं, नयी कार्य योजनायें और कार्यक्रम बनते हैं, पर सवाल है कि उनका समीक्षाओं का आधार क्या होता है और क्या उन चर्चाओं में इस विसंगति पर कोई सवाल नहीं उठता?
स्वतंत्रता के बाद से भारत में विकास के नीतियों में बड़ी विकास परियोजनाओं (बाँध, सड़क, बिजलीघर आदि) का बड़ा महत्त्व रहा है. पंडित नेहरु ने कहा था कि बाँध तो विकास के तीर्थ हैं. इन तीर्थों की स्थापना के कारण एक बड़ी आबादी विस्थापित होती है. 1950 से 1999 के बीच 5835 बड़ी और माध्यम विकास परियोजनाएं बनी और लागू हुई, जबकि 1999 से 2013 के बीच 21334 बड़ी और माध्यम विकास परियोजनाएं बनीं. इनमें से 6829 में लोगों की बड़ी संख्या में विस्थापन होना तय था, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर योजना आयोग या सम्बंधित विभाग या प्रधानमंत्री कार्यलय (क्योंकि ये परियोजनाएं किसी एक विभाग से ही सम्बंधित नहीं है, इसलिए किसी एक को समन्वय आधारित भूमिका निभाना जरूरी था) ने ऐसी पहल नहीं की, जिसके तहत एक डेश-बोर्ड हो ताकि यह पता चल सके कि इन तमाम परियोजनाओं से किस राज्य के किस जिले में कौन से इलाके में कितने परिवार विस्थापित हो रहे हैं या परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं, उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गयी है, कितनों का पुनर्वास हो गया है और कितनों का पुनर्वास बाकी है? बड़ी विकास परियोजनाओं की वकालत करने वाली सभी सरकारें विस्थापितों के हितों और हकों का संरक्षण करने में अरुचि रखती रही हैं, यही कारण है कि देश के सामने आज भी कोई ऐसा नाकड़ा नहीं है, जिससे पता चले की विकास ने कितनों को विस्थापित किया है? जाने-माने समाजशात्री प्रोफ. वाल्टर फर्नांडीस ने एक आंकलन किया और बताया कि वर्ष 1947 से 2000 के बीच भारत में 10 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ, जिनमें से 6 करोड़ दलित-आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रहते थे. क्या इसका मतलब यह है कि चूंकि विस्थापन केवल आदिवासियों, दलितों और गाँव में रहने वालों के लिए बड़ी विभीषिका लाता है, इसलिए जानबूझ कर विश्वसनीय आंकड़ों के प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं बनायीं है?
मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर एक और चुनौती देता हूँ. देश में लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए बहुत जोरदार मंचबाज़ी हो रही है. स्वास्थ्य की एक ही परिभाषा है, पर उस परिभाषा को लागू करने के लिए अभी देश-प्रदेशों में 367 योजनायें चल रही हैं. कौन सी योजना कब शुरू होती है और कब बंद हो जाती है, इसके विषय में शायद ही किसी की पता चलता हो! स्वास्थ्य विभाग के सचिव को भी इसके बारे में कुछ अता-पता नहीं होता है, क्योंकि वो जब विभाग में आता है, तो उसे पता चलता है कि वहां स्वास्थ्य का कोई ठीक-ठीक परिस्थिति विश्लेषण ही मौजूद नहीं है, तो अपनी विद्वत्ता के आधार पर राजनीतिक लाभ-हानि का जोड़-घटना करते हुए वह कोई नयी फंडा-आधारित योजना चला देता है, जो उसके अपने कार्यकाल तक ही जीवित रहती है, पर नयी अधिकारी के आने से पहले दम तोड़ देती है. बस मध्यप्रदेश का एक सन्दर्भ ले लीजिये. राज्य में आप यह जानकारी इकठ्ठा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ सरकारी अस्पतालों-स्वास्थ्य केन्द्रों-चिकित्सा महाविद्यालयों (जो सरकार चलाती है) में अलग-अलग स्तरों के स्वास्थ्य केन्द्रों (उप-स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक, स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मुख्य अस्पताल आदि) के लिए अलग-अलग जिलों में डाक्टरों और विशेषज्ञों कितने पद स्वीकृत स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद भरे हुए हैं या खाली हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का महकमा स्वास्थ्य संचालनालय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा शिक्षा जैसी इकाईओं में बंटा हुआ है, जो केवल अपने हिस्से की व्यापक जानकारी ही रखते हैं. उनके पास भी जिलों यानी जमीनी स्तर की स्पष्ट जानकारी नहीं होती है. आंकड़ों की बात होने पर उनका जवाब होता है कि जिन्हें ये जानकारी चाहिए, वे जिले-जिले जाएँ और वहां से जानकारी इकठ्ठा कर लें. यही संकट दवाओं और अन्य विशेष सेवाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है. जब हमें किसी जिले के बारे में यही पता न चले कि वहां स्वास्थ्य से जुड़े मानव संसाधनों की क्या स्थिति है, तो कार्ययोजना कैसे बन सकती है; पर हमारे यहाँ बनती है और क्रियान्वित भी होती है और सही समय पर उसके लागू हो जाने की रिपोर्ट भी आ जाती है.
जब तक हमारे पास सही सही जानकारियां नहीं होंगी, तब तक क्या समावेशी विकास के बात महज एक मुहावरा नहीं बना रहेगा. वास्तव में चूंकि एक नयी सरकार सत्ता की जिम्मेदारी संभाल रही है, उसे यह समझना होगा कि जब तक सही-सही जानकारी उसके पास या लोगों के पास नहीं होगी, तब तक “समावेशी विकास” और “गैर-बराबरी ख़त्म” करने की कोशिशें नाकाम ही साबित होंगी.
Mr. Sachin Kumar Jain is a development journalist and researcher who is associated with the Right to Food Campaign in India and works with Vikas Samvad, AHRC’s partner organisation in Bhopal, Madhya Pradesh. The author could be contacted at sachin.vikassamvad@gmail.com Telephone: +91 755 4252789.